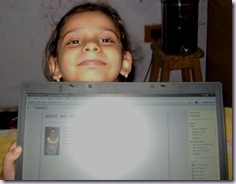सुन्दरलाल बहुगुणा कहते हैं कि उनकी जिन्दगी के दौरान ही गंगा में पानी आधा हो गया। अखबार में उनकी फोटो में सन जैसे सफेद दाढ़ी मूछों वाला आदमी है। मैं बहुगुणा को चीन्हता हूं। पर वे अब बहुत बूढ़े लगते हैं चित्र में। वे चिपको अन्दोलन के चक्कर में अखबार में आते थे। और मैं उन्हे एक जबरी विचार ठेलक (thought pusher) समझता था। कालान्तर में उनके प्रति इज्जत बढ़ गयी – वैसे ही जैसे अपने को मैं कुछ काम का समझने लगा!

मैं अखबार देखता हूं। उडते सूअरों का आतंक और सौन्दर्य का दमकता रूप - यही दीखता है। मैं शाम को फोर्ट एरिया में जाता हूं, फुटपाथ पर किताबें छानने। मुंह पर मास्क लगाये युवक-युवतियों को देखता हूं। मैं सोचता हूं कि समय जिनके साथ है वे भय में क्यों हैं? उसके बाद फोर्ट एरिया, नरीमन प्वॉइण्ट और चचगेट में मास्क लगाये बूढ़े खोजता हूं - मुझे मिलते नहीं।

जैसी टिप्पणियां मिल रही हैं, उनपर ध्यान दें - अरविन्द मिश्र जी मुझे वैराज्ञ की ओर मुड़ा बताते हैं – वे इशारा करती हैं कि पण्डित ज्ञानदत्त पांड़े, थोड़ा हिन्दी अंग्रेजी जोड़ तोड़ कर लिख भले रहे हो तुम; पर मूलत: गये हो सठिया।
इसके अलावा ये जवान लोग चच्चा, कक्का बताये चले जा रहे हैं। शुक्र है किसी महिला ने अभी तक ऐसा नहीं कहा वर्ना जिम ज्वाइन कर वजन कम करना और फेशियल मसाज का अतिरिक्त खर्चा वहन करना बजट में शामिल हो जाये। और उस बजट को मेरी पत्नी कदापि सेंक्शन नहीं देंगी, वैसे ही जैसे एक कोडल लाइफ के बाद किसी वैगन के ओवरहॉल पर पैसा खर्च नहीं किया जाता!
महाकवि केशव की स्थिति समझ में आती है जिन्हे छोरियां बाबा कह कह चली जा रही थीं। मुझे आशा है कि गिरिजेश राव और कृष्ण मोहन मिश्र जैसे जवान यह इशारा नहीं कर रहे कि बहुत हो गया अंकल जी, अब दुकान बन्द करो!
इस समय लम्बी बैठकों और भारतीय रेल के माल यातायात में बढ़ोतरी की स्ट्रेटेजी की सोच से संतृप्त हो चुका है शरीर-मन। दो दिन की बड़ी बैठक के लिये यात्रा खलने लगी है। बड़ा अच्छा हो जब ये सब बैठकें टेली-कॉंफ्रेसिंग से होने लगें।
जब सवेरे यह पोस्ट खुलेगी तो वापसी की मेरी गाड़ी ताप्ती-नर्मदा के आसपास होगी। मेरी स्मृति में जळगांव की कपास मण्डी में कपास का ढेर आ रहा है जो मैने नौ साल पहले देखा था!
(महानगरी एक्स्प्रेस के रेक प्लेसमेण्ट की प्रतीक्षा में १३ अगस्त की रात में मुम्बई वीटी स्टेशन के रेस्ट हाउस से ठेली गई पोस्ट।)
@@@@@@@
यात्रा में टिप्पणी निर्वहन धर्म
(यह पोस्ट मैने १२ अगस्त की सवेरे पब्लिश करने को लिखी थी। पर पब्लिश नहीं किया क्यों कि इसके फॉलो-अप/माडरेशन के लिये समय न निकलता। अब इसे डिलीट करने की बजाय साथ में नत्थी कर दे रहा हूं।)

जब मैं उठा तो दिन शुरू हो गया था। एक स्टेशन के पास पानी भर रहे थे लोग।
मैने यात्रा में चलताऊ मोबाइल कनेक्शन से अपनी पोस्ट बनाने और पब्लिश करने का काम सफलता से कर लिया। कुछ टिप्पणियां भी देख-पब्लिश कर लीं। अन्य लोगों के ब्लॉग पढ़ना और टिप्पणी करना कुछ कठिन काम है। पन्ने खुलते ही नहीं और उन्हें खोल-पढ़ कर टिप्पणी करना असंभव है यात्रा में आते-जाते इण्टरनेट कनेक्शन से। कैसे किया जा सकता है? मेरे विचार से एक बड़े जंक्शन स्टेशन पर जब आपकी गाड़ी रुकी हो; गूगल गीयर्स के माध्यम से अपना गूगल रीडर्स ऑफ लाइन इस्तेमाल के लिये डाउनलोड कर लेना चाहिये। उसमें चित्र नहीं आ पाते और अगर लोग अपनी पूरी फीड नहीं देते तो पढ़ने में पूरा नहीं आ पाता। पर फिर भी पर्याप्त अन्दाज लग जाता है कि लोग क्या कह रहे हैं।
और तब इत्मीनान से गूगल रीडर में ऑफलाइन पोस्ट पढ़ कर एक पोस्ट अनूप शुक्ल की चिठ्ठा-चर्चा के फॉर्मेट में लिख-पब्लिश कर टिप्पणी-निर्वहन-धर्म का पालन कर सकते हैं। पोस्टों को लिंक देने में कुछ झंझट हो सकता है – जब वे फीड्बर्नर के माध्यम से मिलती हों। पर फिर भी ठीकठाक काम हो सकता है।
देखा जाये।
(वैसे कल (१२ अगस्त) मेरे लिये बहुत व्यस्त दिन है। लिहाजा इसे पोस्ट न करना ही उपयुक्त होगा।)
मां बाप एक ऐसा घना पेड होता है जिस की छाव नसीब वालो को मिलती है, राज भाटिया जी से असहमत होने का प्रश्न नहीं। पूत कुपूत होता है, माता कुमाता नहीं होती। उनको हुये मातृशोक पर संवेदना।
रंजन जी ने स्काई और मेट्रो की तुलना की है। अंत में वोट देने को नहीं कहा। अन्यथा मैं मेट्रो को देता। मेट्रो के ई. श्रीधरन किसी जमाने में मेरे महाप्रबन्धक रह चुके हैं – पश्चिम रेलवे में। और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं।
संजीत त्रिपाठी राजनीति में जुड़े लोगों के समृद्ध होने की बात कहते हैं। मुझे भी लगता है राजनीति ट्राई करनी चाहिये थी। यह अवश्य है कि मेरा ई.क्यू. (इमोशनल कोशेंट) उस काम के स्तर का नहीं है।
पर्यावरण पर कलम में जताई चिंता बहुत जायज है। और मेरा मत है कि इस विषय पर हिन्दी में बहुत कम लिखा जा रहा है।
अरविन्द मिश्र जी आभासी दुनियां के विषय में विचार व्यक्त करते हैं कि मानवीयता का क्षरण होगा इससे। मेरा अपना उदाहरण है कि इस वर्चुअल दुनियां के चलते मैं बहु आयामी देख-पढ़-अभिव्यक्त कर रहा हूं। यह तो औजार है – प्रयोग आसुरी भी सम्भव है और दैवीय भी।
संगीता पुरी जी मौसम और गत्यात्मक ज्योतिष की बात करती हैं। हमें अभी दोनो ही पहेली लगते हैं!
ताऊ की साप्ताहिक पत्रिका में उनका फोटो नहीं समीर लाल जी का जरूर दिखता है!
सीबीआई के पास पिल्ले ही नहीं बहुत कुछ होता है। एच.एम.वी. का रिकार्ड बजाते हैं पिल्ले! – काजल कुमार के कार्टून पर रिस्पॉंस!
रेणु शैलेंद्र और पवई लेक – कभी पवई लेक गया नहीं। काश आईआईटी मुम्बई में पढ़ा होता! सतीश पंचम बहुत कीमती ब्लॉगर हैं!
विवेक रस्तोगी जी से पूर्ण सहमति माता-पिता के विषय में जो उन्होने कहा।
गिरिजेश राव को पढ़ते समय फणीश्वर नाथ रेणु की याद आती है। कितनी सशक्त है लेखनी। बस यह है कि पोस्ट के आकार में सिमटती नहीं।
मेहनत के लिये हो गर तैयार, तो चलो ।
एक ठान ली है जब, तो उसी राह पर बढो --- जब आशा जोगलेकर जी यह कहती हैं तो बहुत युवा प्रतीत होती हैं। उम्र का अंदाज करें।
सुनामी वह अध्याय है जिसकी सोच मुझे अपनी निष्क्रियता पर खेद होता है। मुझे पूरी सहानुभूति थी, पर किया कुछ नहीं। तनख्वाह से कुछ कट गया था, बस। दिनेश राय द्विवेदी जी की पोस्ट पर कविता पढ़ कर वही याद हो आया।
संजय व्यास एक प्यारी कलम के मालिक हैं। पार्क पर लिखते वे जो गहराई दिखाते हैं पोस्ट में , वह अत्यन्त प्रशंसनीय है।
मैं जारी रख सकता हूं, पर चलती ट्रेन के झटकों में लिखने की अपनी सीमा है! उम्र से जोड़ सकते हैं इस सीमा को आप।
आशा है शिव कुमार मिश्र का बैक पेन कम होगा। लिखा नहीं उन्होने कुछ। और दो जवान लोगों की कलम से स्नेह होता है – ये बहुत नई उम्र का लिखते हैं – कुश और अनिल कान्त