कुछ समय पहले मै खुडमुडी गाँव के श्री नगेसर से बात कर रहा था। उसे हम लोग बचपन ही से जानते हैं। मेहनत-मजदूरी कर पेट पालने वाला नगेसर अपने गठीले बदन के कारण गाँव मे लोकप्रिय रहा। इस बार वह एकदम बदल गया था। दो साल पहले जब वह बरसात के दिनो मे अपने दो साथियो खेत से लौट रहा था तभी बिजली गिर गयी। उसके दो साथी वहीं पर मर गये। नगेसर को ज्यादा शारीरिक क्षति नही हुयी पर मन से वह पूरी तरह खोखला हो गया।
ऐसे पेड़ जिनकी मूसला जड़ें अधिक गहरी नही जाती और दूसरी जड़ें सतह के पास फैली होती है बिजली से इंसानो की रक्षा कर सकते है। वैज्ञानिक कहते है कि जड़ों का मकडजाल चार्ज को डिफ्यूज कर देता है। इसलिये बिजली से बचने के लिये घर के आस-पास सागौन के पेड लगाने की सलाह दी जाती है।

श्री पंकज अवधिया का लेख। आप उनके लेख
पंकज अवधिया लेबल सर्च में देख सकते हैं।
शरीर का कुछ भाग काला पड गया। मुझसे उसे जडी-बूटी की उम्मीद थी। मैने उसे परसा (पलाश) की लकडी दी और उसका पानी पीने को कहा। मैने उसे कुछ हर्बल मालाएँ भी दी। मुझे मालूम है कि ये जडी-बूटियाँ उसे बाहर से ठीक कर देंगी लेकिन मन की पीडा को वह आजीवन भोगता रहेगा।
बचपन मे घर के पास एक नीम के पेड़ पर बिजली (गाज) गिरी थी। उस चमक से डरकर मै कुछ समय के लिये बेसुध हो गया था। तब से मुझे आसमानी बिजली के कड़कने के समय बहुत भय लगता है। होम्योपैथी मे फास्फोरिकम नामक दवा के मरीज को तूफानो से बहुत डर लगता है मेरी तरह।
शहरो मे विभिन्न उपाय अपना कर हम आसमानी बिजली से काफी हद तक बच जाते है पर हमारे किसान बरसात मे खुले मे खेतों मे काम करते है। पानी से भरे धान के खेत आसमानी बिजली को आमंत्रित करने मे कोई कसर नही छोडते हैं। हर साल अनगिनत किसान और खेतीहर मजदूर आसमानी बिजली के गिरने से बेमौत मारे जाते हैं। उनके पास सुरक्षा के कोई कारगर उपाय नही है।

इस वियतनामी किसान को देखें। जो सिर पर बांस की छीलन से बनी दउरी पहने है, वह
खुमरी सा है। उसके दोनो हाथ काम करने को मुक्त हैं।
फोटो विकीमेडिया से।
लोहे की डंडी वाले छाते आसमानी बिजली को आमंत्रित कर सकते हैं। पर यह संतोष की बात है कि ज्यादातर किसान अभी भी बाँस से बनी खुमरी (यह लिंक देखें) का प्रयोग करते हैं। खुमरी के कारण उनके दोनो हाथ काम करने के लिये स्वतंत्र होते हैं। किसान पेड़ों की शरण लेते हैं। यह जानते हुये भी कि बरसात के दिनो मे पेड़ों की शरण घातक सिद्ध हो सकती है।
क्या कोई विशेष पेड है जिस पर बिजली ज्यादा गिरती है? आप भले ही इस प्रश्न पर हँसे पर छत्तीसगढ के लोग महुआ, अर्जुन और मुनगा (सहजन) का नाम लेते है। उनका यह अनुभव विज्ञान सम्मत भी है। वैज्ञानिक शोध सन्दर्भ बताते है कि ऐसे बडे पेड़ जिनकी जड़ें भूमिगत जल तक पहुँचती हैं, उन पर बिजली गिरने की सम्भावना अधिक होती है। हमारे यहाँ 50-60 फीट गहरा कुँआ खोदने वाले कुछ तमिलनाडु के लोग हैं। वे उन पेड़ों के पास कुँआ खोदने के लिये तैयार हो जाते है जिन पर बिजली गिरी होती है। ऐसे पेड़ जिनकी मूसला जड़ें अधिक गहरी नही जाती और दूसरी जड़ें सतह के पास फैली होती है बिजली से इंसानो की रक्षा कर सकते है। वैज्ञानिक कहते है कि जड़ों का मकडजाल चार्ज को डिफ्यूज कर देता हैं। इसलिये बिजली से बचने के लिये घर के आस-पास सागौन के पेड लगाने की सलाह दी जाती है।
यदि आप खुली जगह मे हैं तो मौसम खराब होते ही झुककर बैठ जायें। झुककर बैठने का उद्देश्य सतह पर दूसरी चीजो की तुलना मे अपनी ऊँचाई कम करना है ताकि बिजली आप पर गिरने की बजाय ऊँची चीज पर गिरे। फैराडे के किसी नियम के अनुसार बन्द बक्सों मे बिजली नही गिरती है। यही कारण है कि गाड़ियों मे बिजली नही गिरती। पर किसान के लिये झुककर बैठना सम्भव नही है। आखिर वह कब तक बैठा रहेगा। खेतो के पास यदि सस्ते मे बन्द बाक्स बना दिये जाये तो भी किसान अन्दर नही बैठ सकता। यह व्यवहारिक उपाय नही है।
प्राचीन भारतीय ग्रंथ कहते है कि तुलसी की माला बिजली से शरीर की रक्षा करती है। यह भी कि जिस पर बिजली गिरी हो उसे तुलसी की माला पहननी चाहिये। दूसरी बात मुझे सही लगती है। मै ये अपने अनुभव से कह रहा हूँ। तुलसी की माला पहनने से बिजली नही गिरेगी - इसे आधुनिक विज्ञान की कसौटी मे परखना जरुरी लगता है।
पारम्परिक चिकित्सको के लिये जंगली पेडो पर बिजली गिरना किसी वरदान से कम नही है। जितनी जल्दी हो सके वे प्रभावित पेड तक पहुँचते है और लकडी एकत्र कर लेते है। इस लकडी का प्रयोग असाध्य रोगों की चिकित्सा मे होता है। इस पर आधारित एक लेख आप यहाँ पढ सकते है।
Lightening is beneficial too. By Pankaj Oudhia
ज्ञानदत्त जी के ब्लाग में किसान से जुडी इस महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य ब्लाग पर आने वाले प्रबुद्ध पाठकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है। मुझे विश्वास है कि किसानों को आसमानी बिजली के कहर से बचाने के लिये कारगर उपायों पर आपके विचारो से हम किसी ठोस निष्क़र्ष तक जरुर पहुँच पायेंगे। वैसे पारम्परिक चिकित्सक कहते हैं कि किसानो से ज्यादा खतरनाक परिस्थितियो मे खराब मौसम के दौरान बन्दर रहते हैं। पानी से भीगे पेड़ों मे वे मजे से रहते है। क्या कभी बन्दरो को आसमानी बिजली से मरते देखा है या सुना है? बन्दरों के पास समाधान छुपा है। मुझे उनकी बात जँचती है। यहाँ सारा मानव जगत सर्दी से त्रस्त होता रहता है वहीं दूसरी ओर यह वैज्ञानिक सत्य है कि बन्दरो को सर्दी नही होती।
पंकज अवधिया
(इस लेख का सर्वाधिकार श्री पंकज अवधिया के पास है)




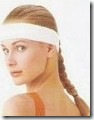















 मेरी पत्नी जी का झोला।
मेरी पत्नी जी का झोला।

