मेरी पत्नीजी अपने परिवेश से जुड़ना चाहती थीं – लोग, उनकी समस्यायें, मेला, तीज-त्योहार आदि से। मैने भी कहा कि बहुत अच्छा है। पर यह जुड़ना किसी भी स्तर पर पुलीस या प्रशासन से इण्टरेक्शन मांगता हो तो दूर से नमस्कार कर लो। इस बात को प्रत्यक्ष परखने का अवसर जल्द मिल गया। वह वर्दी वाला पुलिसिया दम्भी अकड़ के साथ बैठा रहा मुहल्ले की मेला-बैठक में। मेरी पत्नीजी ने परिचय कराने पर उसका अभिवादन करने की गलती भी कर ली। [१]
|| MERI MAANSIK HALCHAL ||
|| मेरी (ज्ञानदत्त पाण्डेय की) मानसिक हलचल ||
|| मन में बहुत कुछ चलता है ||
|| मन है तो मैं हूं ||
|| मेरे होने का दस्तावेजी प्रमाण बन रहा है यह ब्लॉग ||
Saturday, November 6, 2010
सर्विसेज
Sunday, October 24, 2010
लल्लू
हमें बताया कि लोहे का गेट बनता है आलू कोल्ड स्टोरेज के पास। वहां घूम आये। मिट्टी का चाक चलाते कुम्हार थे वहां, पर गेट बनाने वाले नहीं। घर आ कर घर का रिनोवेशन करने वाले मिस्तरी-इन-चार्ज भगत जी को कहा तो बोले – ऊंही त बा, पतन्जली के लग्गे (वहीं तो है, पतंजलि स्कूल के पास में)!
यानी भगत जी ने हमें गलत पता दिया था। पतंजलि स्कूल कोल्ड स्टोरेज के विपरीत दिशा में है।
Monday, May 10, 2010
अतिक्रमण हटा; फिर?

इस काम में कई लोग लगे थे, पर हमारी ओर से लगे थे श्री विनोद शुक्ल। पुलीस वालों से और स्थानीय लोगों से सम्पर्क करना, उनको इकठ्ठा करना, समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सहायक बनना – यह उन्होने किया। मैने विनोद शुक्ल को धन्यवाद दिया। एक दिन पहले जब वे बता रहे थे कि कुछ हो नहीं पा रहा है तो वे विलेन नजर आ रहे थे। मैने उन्हे ही नहीं, जाने किन किन को कोसा था।
Monday, March 15, 2010
गंगा किनारे की रह चह
 घर से बाहर निकलते ही उष्ट्रराज पांड़े मिल गये। हनुमान मन्दिर के संहजन की पत्तियां खा रहे थे। उनका फोटो लेते समय एक राह चलते ने नसीहत दी – जरा संभल कर। ऊंट बिगड़ता है तो सीधे गरदन पकड़ता है।
घर से बाहर निकलते ही उष्ट्रराज पांड़े मिल गये। हनुमान मन्दिर के संहजन की पत्तियां खा रहे थे। उनका फोटो लेते समय एक राह चलते ने नसीहत दी – जरा संभल कर। ऊंट बिगड़ता है तो सीधे गरदन पकड़ता है।बाद में यही उष्ट्रराज गंगाजी की धारा पैदल चल कर पार करते दीखे। बड़ी तेजी से नदी पर उग आये द्वीपों को पार करते गये। टापुओं पर लौकी खूब उतरने लगी है। उसका परिवहन करने में इनका उपयोग हो रहा है।
Saturday, March 13, 2010
प्रवीण – जुते हुये बैल से रूपान्तरण
आदरणीया भाभीजी,
पहले आपके प्रश्न का उत्तर और उसके बाद ही ट्रैफिक सर्विस की टीस व्यक्त करूँगा।
Friday, March 12, 2010
बच्चों को पढ़ाना - एक घरेलू टिप्पणी
मेरी पत्नीजी (रीता पाण्डेय) की प्रवीण पाण्डेय की पिछली पोस्ट पर यह टिप्पणी प्रवीण पर कम, मुझ पर कहीं गम्भीर प्रहार है। प्रवीण ने बच्चों को पढ़ाने का दायित्व स्वीकार कर और उसका सफलता पूर्वक निर्वहन कर मुझे निशाने पर ला दिया है।
समस्या यह है कि मेरे ऊपर इस टिप्पणी को टाइप कर पोस्ट करने का भी दायित्व है। खैर, आप तो टिप्पणी पढ़ें:
प्रिय प्रवीण,
मुझे तुमसे पूरी सहानुभूति है। बच्चों की चुनौतीपूर्ण मुद्रा से तो और भी आशंकित हूं। तुम्हारा काम (उन्हे पढ़ाने का) वाकई में दुरुह है। यह मैं अपने अनुभव से बता रही हूं। समय के साथ यह चुनौती प्रबल होती जायेगी।
Monday, March 8, 2010
नत्तू पांड़े, नत्तू पांड़े कहां गये थे?
 नत्तू पांड़े नत्तू पांड़े कहां गये थे?
नत्तू पांड़े नत्तू पांड़े कहां गये थे? झूले में अपने सो रहे थे
सपना खराब आया रो पड़े थे
मम्मी ने हाल पूछा हंस गये थे
पापा के कहने पे बोल पड़े थे
संजय ने हाथ पकड़ा डर गये थे
वाकर में धक्का लगा चल पड़े थे
नत्तू पांड़े नत्तू पांड़े कहां गये थे?!
Saturday, November 7, 2009
थकोहम्
मुझे अन्देशा था कि कोई न कोई कहेगा कि गंगा विषयक पोस्ट लिखना एकांगी हो गया है। मेरी पत्नीजी तो बहुत पहले कह चुकी थीं। पर कालान्तर में उन्हे शायद ठीक लगने लगा। अभी घोस्ट बस्टर जी ने कहा -
लेकिन थोड़े झिझकते हुए कहना चाहूंगा कि मामला थोड़ा प्रेडिक्टेबल होता जा रहा है. ब्लॉग पोस्ट्स में विविधता और सरप्राइज़ एलीमेंट की कुछ कमी महसूस कर रहा हूं।
Monday, August 3, 2009
रेलगाड़ी का इन्तजार

मेरी जिन्दगी रेलगाड़ियों के प्रबन्धन में लगी है। ओढ़ना-बिछौना रेल मय है। ऐसे में गुजरती ट्रेन से स्वाभाविक ऊब होनी चाहिये। पर वैसा है नहीं। कोई भी गाड़ी गुजरे – बरबस उसकी ओर नजर जाती है। डिब्बों की संख्या गिनने लगते हैं। ट्रेन सभी के आकर्षण का केन्द्र है – जब से बनी, तब से। स्टीम इंजन के जमाने में बहुत मेस्मराइज करती थी। डीजल और बिजली के इंजन के युग में भी आकर्षण कम नहीं है। जाने क्यों है यह। मनोवैज्ञानिक प्रकाश डाल सकते हैं।
सवेरे ट्रेन की आवाज आ रही थी। यह लग रहा था कि कुछ समय बाद फाफामऊ के पुल से गुजरेगी। मैं कयास लगा रहा था कि यह दस डिब्बे वाली पसीजर (पैसेंजर)होगी या बड़ी वाली बुन्देलवा (बुन्देलखण्ड एक्स्प्रेस)। अपना कैमरा वीडियो रिकार्डिंग मोड में सेट कर गंगा की रेती में खड़ा हो गया। तेलियरगंज की तरफ से आने वाली रेलगाड़ी जब पेड़ों के झुरमुट को पार कर दीखने लगेगी, तब का वीडियो लेने के लिये। पर अनुमान से ज्यादा समय ले रही थी वह आने में।
रेल की सीटी, पटरी की खटर पटर सुनते सुनते पत्नीजी बोलीं – तुम भी अजब खब्ती हो और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी खड़ा रहना पड़ रहा है। आने जाने वाले क्या सोचते होंगे!
अन्तत: ट्रेन आयी। वही दस डिब्बे वाली पसीजर। दसों डिब्बे गिनने के बाद वही अनुभूति हुई जो नर्सरी स्कूल के बच्चे को होमवर्क पूरा करने पर होती होगी!
यह हाल नित्य 400-500 मालगाड़ियों और दो सौ इन्जनों के प्रबन्धन करने वाले का है, जो सवेरे पांच बजे से रात दस बजे तक मालगाड़ियों का आदानप्रदान गिनता रहता है तो रेलवे से न जुड़े लोगों को तो और भी आकर्षित करती होगी रेल!
अपडेट साढ़े छ बजे -
आज श्रावण का अन्तिम सोमवार है। आज भी चेंचामेची मची है शिवकुटी के कोटेश्वर महादेव मन्दिर पर। संपेरा भी आया है दो नाग ले कर। यह रहा उसका वीडियो:Saturday, July 18, 2009
नत्तू पांड़े का झूला

उनके आते समय उनके कारवां में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मैं तो आगे आगे चल रहा था, वे पीछे रह गये। मुड़ कर देखा तो उनकी नानी उतरते ही उन्हें स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर एक पर अंत में बनी हजरत सैयद करामत अली उर्फ लाइन शाह बाबा की मजार पर प्रणाम करवा रही थीं।
लाइन शाह बाबा की मजार को मैने कभी बहुत ध्यान से नहीं देखा था। नतू पांड़े की मार्फत मेरी धर्मिक आस्था में और विस्तार हो गया। 
नत्तू पांड़े अपना झूला ले कर आये थे। जाली वाला हवादार झूला। उसमें मक्खी-मच्छर नहीं जा सकते। सभी ने उस झूले के साथ बारी बारी फोटो खिंचाई! उसके बाद यहां चौक से उनका नया पेराम्बुलेटर भी आया। सबसे छोटे प्राणी के लिये घर भरा भरा सा लगने लगा।
उनके साथ और सभी ने अपने तरीके से सेवा की और खेले। क्या मौज थी!; पूरा परिवार उनकी चाकरी में लगा था। मेरे साथ उनके कई लम्बे और गहन संवाद हुये। देश की अर्थव्यवस्था से ले कर भूमण्डलीय पर्यावरण, भारतीय दर्शन और भारत के भविष्य के बारे में बहुत मोनोलॉगीय डायलाग हुये। मैं समझता हूं कि उन्होने भविष्य में सब ठीक कर देने की हामी भरी है। उनके इस प्रॉमिस को मुझे बारम्बार याद दिलाते रहना है!
नत्तू पांडे वापस बोकारो के लिये जा चुके हैं। उनके कार्यकलाप अभी भी मन में नाच रहे हैं।
Monday, July 6, 2009
अवसादहारिणी गंगा
 |
 |
 |
 |
उस दिन मेरे रिश्ते में एक सज्जन श्री प्रवीणचन्द्र दुबे [1] मेरी मेरे घर आये थे और इस जगह पर एक मकान खरीद लेने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। मैं घर पर नहीं था, अत: उनसे मुलाकात नहीं हुई।
टूटी सड़क, ओवरफ्लो करती नालियां और सूअरों से समृद्ध इस जगह में वह क्यों बसना चाहते हैं तो मेरी पत्नीजी ने बताया कि “वह भी तुम्हारी तरह थोड़ा क्रैंकी हैं। पैसा कौड़ी की बजाय गंगा का सामीप्य चाहते हैं”।
अब देखें, पत्नीजी भी हमारी क्रैंकियत को अहमियत नहीं देतीं, तो और लोग क्या देंगे! श्री प्रवीणचन्द्र दुबे की पत्नी से नहीं पता किया – शायद वहां भी यही हाल हो!
खैर, शायद यह “बैक ऑफ द माइण्ड” रहा हो - कल सवेरे सवेरे गंगा किनारे चला गया। पांव में हवाई चप्पल डाल रखी थी। गनीमत है कि हल्की बारिश हो चुकी थी, अन्यथा रेती में चलने में कष्ट होता। भिनसारे का अलसाया सूरज बादलों से चुहुल करता हुआ सामने था। कछार में लौकी-नेनुआ-कोंहड़ा के खेत अब खत्म हो चुके थे, लिहाजा गंगामाई की जलधारा दूर से भी नजर आ रही थी।
गंगा स्नान को आते जाते लोग थे। और मिले दो-चार कुकुर, भैंसें और एक उष्ट्रराज। उष्ट्रराज गंगा किनारे जाने कैसे पंहुच गये। मजे में चर रहे थे – कोई मालिक भी पास नहीं था।
गंगा किनारे इस घाट का पण्डा स्नान कर चुका था। वापस लौट कर चन्दन आदि से अपना मेक-अप कर तख्ते पर बैठने वाला था। एक सज्जन, जो नहा रहे थे, किसी जंगली वेराइटी के कुकुरों का बखान कर रहे है - “अरे ओन्हने जबर जंगली कुकुर होथीं। ओनही के साहेब लोग गरे में पट्टा बांधि क घुमावथीं” (अरे वे जबर जंगली कुत्ते होते हैं। साहेब लोग उन्ही को पालते हैं और गले में पट्टा बांध कर घुमाते हैं)। शरीर के मूल भाग को स्नानोपरान्त गमछा से रगड़ते हुये जो वे श्वान पुराण का प्रवचन कर रहे थे, उसे सुन मेरा अवसाद बेबिन्द (पगहा तुड़ा कर, बगटुट) भागा!
गंगामाई में थोड़ा और जल आ गया है और थोड़ा बहाव बन गया है। अच्छा लगा। मैं तो ग्रीष्मकाल की मृतप्राय गंगा की छवि मन में ले कर गया था; पर वे जीवन्त, अवसादहारिणी और जीवनदायिनी दिखीं।
जय गंगामाई!
[1] मुझे बताया गया; श्री प्रवीण चन्द्र दुबे रीवां में चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं। मैं उनसे आमने सामने मिला नहीं हूं (अन्यथा यहां उनका चित्र होता जरूर)। वे अब इन्दौर जायेंगे स्थानान्तरण पर। उनके प्रभाव क्षेत्र में इदौर-झाबुआ-धार के जंगल रहेंगे। और मैं वह मालव क्षेत्र एक बार पुन: देखना चाहूंगा!
प्रवीण, जैसा मुझे बताया गया, एस्ट्रॉलॉजी में गहरी दखल रखते हैं। किसी को प्रभावित करने का ज्योतिष से कोई बढ़िया तरीका नहीं!
Thursday, July 2, 2009
सरकते बॉटलनेक्स (Bottlenecks)
जहां कहीं कतार लगी दिखे तो मान लीजिये कि आगे कहीं बॉटलनेक है। बॉटलनेक माने बोतल की संकरी गर्दन। किसी असेम्बली लाइन या यातायात व्यवस्था में इसके दर्शन बहुधा होते हैं। रेलवे आरक्षण और पूछताछ की क्यू में इसके दर्शन आम हैं। बॉटलनेक कैसे दूर करें?
अगर सिस्टम बहुत जटिल है तो उसमें बॉटलनेक को चिन्हित करना ही कठिन काम है। बड़े बड़े प्रबन्धन के दिग्गज इसमें गलतियां कर जाते हैं। किसी भी शहर के सड़क यातायात प्रबन्धन के सिस्टम मुझे ज्यादा जटिल नहीं लगते। पर नई कालोनियां कैसे आ रही हैं, लोग कैसे वाहन पर चलेंगे आने वाले समय में। नये एम्प्लायर्स कहां सेट-अप कर रहे हैं अपना उपक्रम – यह सब ट्रैफिक प्लानिंग का अंग है। और इस प्लानिंग में चूक होना सामान्य सी बात है।
अभी पढ़ा है कि वर्ली-बान्द्रा समुद्र पर लिंक बना है। यह दूरी और समय कम कर रहा है। यह पढ़ते ही लगा था कि अगर यातायात प्लानर्स ने बॉटलनेक्स पर पूर्णत: नहीं सोचा होगा तो बॉटलनेक दूर नहीं हुआ होगा, मात्र सरका होगा। और वैसा ही निकला।
बिजनेस स्टैण्डर्ड के इस सम्पादकीय पर नजर डालें:
…
महाराष्ट्र सरकार ने दोनों बिन्दुओं के बीच 7.7 किलोमीटर की दूरी को 7 मिनट में पूरा करने का वादा किया था। लेकिन सरकार के ज्यादातर वादों की तरह यह भी एक अधूरा सपना होकर रह गया है।
… हालांकि इससे व्यस्त समय में मौजूदा सड़क मार्ग पर लगने वाले जाम में भारी सुधार आएगा, लेकिन समस्या उस जगह पर शुरू होगी जहां सी लिंक वर्ली सीफेस पर 90 अंश के कोण पर मिलता है।
दक्षिण और केंद्रीय कारोबारी जिलों को जोड़ने वाले लव ग्रोव जंक्शन तक 1 किलोमीटर लंबे रास्ते पर गति की अधिकतम सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस बीच पांच ट्रैफिक सिग्नल और इतनी ही संख्या में डायवर्जन और मोड़ हैं।
अंतिम दौर में ही 10 से 15 मिनट तक का समय लग सकता है, और इस कारण सी लिंक पर यातायात बाधित हो सकता है।
अब लगता है न कि बॉटलनेक सरका भर है। मैं इसके लिये उन लोगों को दोष नहीं देता। मालगाड़ी के यातायात में मैं भी ऐसी समस्याओं के समाधान तलाशता रहता हूं। और बहुधा बॉटलनेक्स दूर कर नहीं, वरन सरका-सरका कर ही समाधान निकलते हैं। आखिर अकुशल प्रबन्धक जो ठहरा!
इस थियरी ऑफ बॉटलनेक्स/कन्स्ट्रैण्ट्स (Theory of bottleneck/constraints) के बारे में मैं रेलवे में अपने ४० कार्य-घण्टे लगा कर एक प्रवचन लोगों को दे चुका हूं। आप जानकारी की उत्सुकता रखते हों तो यह विकीपेडिया का लिंक खंगालें। मेरे प्रवचन का कभी मैने हिन्दी अनुवाद किया तो प्रस्तुत करूंगा।
मेरी पत्नीजी का कहना है कि बनारस के सड़क के बॉटलनेक्स तो सरकते भी नहीं। बीच सड़क के सांड़ की तरह अड़ कर खड़े रहते हैं। ज्यादा बोलो तो कहते हैं - हम इंही रहब! का तोरे बाप क सड़क हौ!
Monday, June 22, 2009
वृक्षारोपण ॥ बाटी प्रकृति है
 |  पण्डित शिवानन्द दुबे |
मेरे श्वसुर जी ने पौधे लगाये थे लगभग १५ वर्ष पहले। वे अब वृक्ष बन गये हैं। इस बार जब मैने देखा तो लगा कि वे धरती को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान कर गये थे।
असल में एक व्यक्ति के पर्यावरण को योगदान को इससे आंका जाना चाहिये कि उसने अपने जीवन में कितने स्टोमैटा कोशिकाओं को पनपाया। बढ़ती कार्बन डाइ आक्साइड के जमाने में पेड़ पौधों की पत्तियों के पृष्ठ भाग में पाये जाने वाली यह कोशिकायें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और पण्डित शिवानन्द दुबे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिये भी पुण्य दे गये हैं।
वे नहीं हैं। उनके गये एक दशक से ऊपर हो गया। पर ये वृक्ष उनके हरे भरे हस्ताक्षर हैं! क्या वे पर्यावरणवादी थे? हां, अपनी तरह के!
खेती में उन्होने अनेक प्रकार से प्रयोग किये। उस सब के बारे में तो उनकी बिटिया जी बेहतर लिख सकती हैं।
बाटी प्रकृति है:
इन्ही पेड़ों की छाया में रात में बाटी बनी थी। बाटी, चोखा और अरहर की दाल। भोजन में स्वाद का क्या कहना! यह अवसर तीन साल बाद मिला था। फिर जाने कब मिले।
पर यह “फिर जाने कब मिले” की सोचने लगें तो किसी भी आनन्द का खमीरीकरण हो जाये!
अमृतलाल वेगड़ जी के शब्दों में कहूं तो बाटी प्रकृति है, रोटी संस्कृति और पूड़ी विकृति! रात में खुले आसमान में सप्तर्षि तारामण्डल निहारते बाटी की प्रकृति का आनन्द लिया गया!
Sunday, May 31, 2009
पेपर या प्लास्टिक के थैले?
यह मेरे मनपसन्द विषय पर रीडर्स डाइजेस्ट से लिया गया मसाला है। चूंकि अब सर्वोत्तम नहीं छपता और मैं यह अंग्रेजी नहीं हिन्दी में प्रस्तुत कर रहा हूं – अत: मेरे विचार से यह चुरातत्वीय होते हुये भी चल जायेगा।
 मेरी पत्नी जी का झोला।
मेरी पत्नी जी का झोला।वैसे भी शब्द मेरे अपने हैं – रीडर्स डाइजेस्ट के नहीं।
प्लास्टिक के थैलों के निमाण में खनिज तेल का प्रयोग होता है। तेल का उत्खनन, शोधन और अन्तत: प्लास्टिक थैले बनाने में बहुत झंझटीय तकनीकी जरूरी है। पर वही हाल लकड़ी से कागज और कागज के थैले बनाने में है। कागज की मिलें भी अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग और श्वांस की बीमारियां बढ़ाती हैं। और कागज बनाने में बहुत सी ऊर्जा और जल लगता है। कागज के थैले प्लास्टिक के थैलों से छ गुना ज्यादा वजनी होते हैं। अत: उनका परिवहन भी ईंधन मांगता है और जहरीली गैसें उत्सर्जित करता है।
और अगर आप कहते हैं कि प्लास्टिक लैंण्डफिल में नष्ट नहीं होता और कागज हो जाता है, तो भी आप सही नहीं हैं। लैण्डफिल में लगभग कुछ भी विघटित नहीं होता। इनमें कचरा हवा और जल से अछूता रखा जाता है - जिससे धरती का जल प्रदूषित न हो। और जो बायो-डीग्रेडेबल है; वह भी दसियों या सैकड़ों साल ले लेगा। यह होने में वह मीथेन गैस भी छोड़ेगा जो ग्लोबल वार्मिंग करेगा ही।
रीडर्स डाइजेस्ट उवाच:
पेपर या प्लास्टिक के थैले – दोनो ही बेकार विकल्प हैं। आप तो अपने पुन: इस्तेमाल होने वाले जूट या कपड़े के थैले का प्रयोग करें।
विजय का एक कदम?!
Friday, April 3, 2009
सरकारी नौकरी महात्म्य
नव संवत्सर प्रारम्भ हो चुका है। नवरात्र-व्रत-पूजन चल रहा है। देवी उपासना दर्शन पूजा का समय है। ज्ञान भी तरह तरह के चिन्तन में लगे हैं – मूल तत्व, म्यूल तत्व जैसा कुछ अजीब चिन्तन। पारस पत्थर तलाश रहे हैं।

श्रीमती रीता पाण्डेय की पोस्ट। एक निम्न-मध्यवर्गीय यूपोरियन (उत्तरप्रदेशीय) माहौल में सरकारी नौकरी का महत्व, पुत्र रत्नों की आवश्यकता और दहेज के प्रति जो आसक्ति दीखती है - वह अनुभूत सत्य उन्होंने आज लिखा है।
मैं ही छुद्र प्राणी हूं। छोटी-छोटी पारिवारिक समस्याओं में उलझी हूं। कूलर का पंखा और घास के पैड बदलवाये हैं आज। भरतलाल की शादी होने जा रही है। उसकी पत्नी के लिये साड़ी कहां से खरीदवाऊं, अटैची कौन से रंग की हो। इन छोटे छोटे कामों में ही जीवन लगे जा रहा है। व्यर्थ हो रहा है जीवन। मुझे इससे ऊपर उठना ही होगा।
यह सोच जैसे ही मैने सिर ऊपर उठाया – एक महान महिला के दर्शन हुये। वे नवरात्र का नवदिन व्रत करती हैं। रोज गंगा स्नान करती हैं। पैदल जाती हैं। मुहल्ले की रात की शांति की परवाह न करते हुये रात्रि जागरण करवाती हैं। उनके ही अनुसार उन्हें धन का तनिक मोह नहीं है। जो कुछ धन था, उसका सदुपयोग कर घर का फर्श-दीवार संगमरमर से मिढ़वा दिया है। घर ताजमहल बन गया है। सब उनके पति की सरकारी नौकरी का महात्म्य है!
भगवान की कृपा से उनके अनेक हीरे हैं। प्रत्येक को तलाशते कई मोतियों के अभिभावक दहेज नामक मैल की थैलियां लिये घूम रहे हैं। उनकी समस्या है कि किस मोती और कितने मैल को स्वीकार करें। वे बात बात में एक दूसरी महिला को ज्ञान बांटती हैं – “अरे अब तुम्हारे पति की सरकारी नौकरी लग गयी है, अब एक बच्चे पर क्यों रुक रही हो। अब तो इत्मीनान से पैदा करो।”
इतने महत्वपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर दिया है मुझे कि इस ज्ञान को सर्वत्र फैलाने का मन हो रहा है। भारत के नव युवक-युवतियों उठो, सरकारी नौकरी पर कब्जा करो और हिन्दुस्तान की धरती को पुत्र रत्नों से भर दो। भविष्य तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का है। उनके माध्यम से सब संपदा तुम्हारी होगी!
जय हिन्द! जय जय!
श्रीमती रीता पाण्डेय का उक्त धर्मनिष्ठ महिला के विषय में पोस्ट स्क्रिप्ट - पुछल्ला:
फलाने की अविवाहता बिटिया गंगा में डूब गयी थी। दुखद प्रसंग था। पर चर्चा चलने पर इन दिव्य महिला ने कवित्त बखाना:
बिन मारे दुसमन मरे, खड़ी ऊंख बिकाय।
बिन ब्याही कन्या मरे, यह खुशी कहां समाय॥
Monday, March 9, 2009
एक गृहणी की कलम से
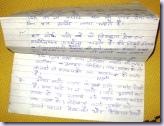

यह एक बड़ी सच्चाई है कि पुरुष या पति यह जानता ही नहीं कि स्त्री (या उसकी पत्नी) उससे किस प्रकार के सहयोग, स्नेह या सम्मान की अपेक्षा करती है। पर यही सच्चाई स्त्रियों के सामने भी प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ी है कि क्या उन्हें पता है कि उन्हें अपने पति से किस तरह का सहयोग चाहिये? हमें पहले अपने आप में यह स्पष्ट होना चाहिये कि हम अपने पति से क्या अपेक्षा रखते हैं।
बहुत गहराई में झांक कर देखें तो स्त्रियां भी वह सब पाना चाहती हैं जो पुरुष पाना चाहते हैं – सफलता, शक्ति, धन, हैसियत, प्यार, विवाह, खुशी और संतुष्टि। पुरुष प्रधान समाज में यह सब पाने का अवसर पुरुष को कई बार दिया जाता है, वहीं स्त्रियों के लिये एक या दो अवसर के बाद रास्ते बन्द हो जाते हैं। कहीं कहीं तो अवसर मिलता ही नहीं।
नारी अंतर्मन की यह पीड़ा और कुछ हासिल कर लेने की अपेक्षा उन्हें एक अनबूझ पहेली के रूप में सामने लाती है। मेरे विचार से अगर हमें यह स्पष्ट हो कि हमें क्या चाहिये तो हमें अपने पति से भी स्पष्ट रूप से कह देना चाहिये कि हम उनसे क्या चाहते हैं -
- हम पति से निश्छल प्रेम का व्यक्तिगत प्रदर्शन चाहते हैं। हमें किसी कीमती उपहार की बजाय उनका हमारी हंसी में हिस्सेदार बनना ही बहुत बड़ा उपहार होगा।
- प्रशंसा एक बहुत बड़ा उपहार है। पत्नी अपनी प्रशंसा सुनना चाहती है। आप घुमा-फिरा कर प्रशंसा करने की बजाय सटीक प्रशंसा कीजिये। प्रशंसा से तो कितनी ही समस्याओं का समाधान हो जाता है।
- औरत अपने काम के प्रति गम्भीर होती है। चाहे गृहस्थी का काम हो या गृहस्थी के साथ साथ बाहर का काम हो। कोई भी कार्य पुरुषों को हैसियत और उनकी पहचान देता है। औरतें भी यही चाहती हैं कि उनके काम को उतना ही महत्व मिले जितना पुरुष अपने काम को देते हैं। कमसे कम पुरुषों को स्त्रियों के काम में रुचि अवश्य दिखानी चाहिये।
- स्त्रियों को सहानुभूति की आवश्यकता होती है। पुरुषों के लिये बातचीत समस्या बताने, व्याख्या करने और समाधान निकालने का औजार है। पर स्त्रियों के लिये बातचीत अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ बांटने और दिल हल्का करने का तरीका है। भावनाओं को कुरेदकर लम्बे संवाद सुनने की अपेक्षा पति से करती है पत्नी – यदि पति में थोड़ा धैर्य हो।
- स्त्रियां समस्याओं का समाधान बहुत अच्छा करना जानती हैं। स्त्रियां और पुरुष अलग अलग ढ़ंग से समस्यायें सुलझाते हैं। पुरुष समस्या पर सीधा वार करता है। सीधा रास्ता चुन कर उसपर चलने का प्रयास करता है। परंतु स्त्रियों के साथ भावनाओं का जाल बहुत घना होता है। वे अपनी समस्याओं को ले कर अड़ नहीं जातीं। समस्याओं को सुलझाने में अपने परिवार को अस्त-व्यस्त नहीं करना चाहतीं। वे अपने समस्या सुलझाने के प्रकार का समर्थन और सम्मान चाहती हैं पुरुष से। वे चाहती हैं कि पुरुष उन्हें कमजोर न समझें।
- घर में रहने वाली गृहणी शायद ही अपने पति से घर का कार्य करवाना चाहेगी। पर दिन भर के काम से थकी पत्नी को पति का स्नेह और सहानुभूति भरा स्पर्श ही ऊर्जा प्रदान कर देगा। और आप रसोईघर में साथ खड़े भर हो जायें आप देखेंगे कि सामान्य सा खाना लजीज व्यंजन में बदल जायेगा। हां, जो स्त्रियां बाहर भी काम करती हैं वे जरूर चाहेंगी कि पति गृहकार्य में बराबर का हिस्सेदार हो। स्त्री को इस बारे में आक्रामक रुख अख्तियार करने की बजाय स्नेह पूर्वक कहना चाहिये।
- स्त्रियां अपने जीवन साथी को सचमुच अपने बराबर का देखना चाहती हैं। ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उनकी भावनाओं का सम्मान करे। संवेदना, सहानुभूति और सुरक्षा का आश्वासन दे।
Thursday, January 8, 2009
विफलता का भय
विफलतायें अन्तत: सफलता में बदलती हैं। न बदलती होतीं तो लिंकन लिंकन न बन पाते। तब विफलताओं का भय क्यों लगता है?
(मैं अपनी कहूं तो) एक भय तो शायद यह है कि पहले असफल होने पर लगता था कि आगे बहुत समय है सफल होने का, पर अब लगता है विफलता चिपक जायेगी। उसके उलट यह भी है कि अब विफलताओं का परिणाम उतना भयावह नहीं होगा। कुल मिला कर अनिष्ट की आशंका समान होनी चाहिये। अंतर शायद यह है शरीर अब असफलता सहने की उतनी क्षमता नहीं रखता। या ज्यादा सही है कि शारिरिक अक्षमता को मनसिक रूप से गढ़ लिया है मैने?!
| मेरी पत्नी मेरे आत्म-धिक्कार की मनोवृत्ति से बहुत खफा हैं। वे मेरी “इनीशियल एडवाण्टेज” न होने की फ्रेजॉलॉजी (phraseology – शब्दविन्यास) को निहायत घटिया सोच मानती हैं। इस पोस्ट की शुरुआत भी मैं उस “इनीशियल डिसएडवाण्टेज” की बात से कर रहा था – और उससे आत्मदया की भावना पर शायद कुछ सहानुभूति युक्त टिप्पणियां मिल जातीं; पर क्या बतायें, इतनी सुबुक-सुबुकवादी धांसूं शुरुआत की रेड़ मार दी रीता पाण्डेय ने! और मेरी हिम्मत नहीं है कि आत्मदया छाप कुछ ठेलने की! |

विफलता का विश्लेषण एक जरूरी अंग है सफलता सुनिश्चित करने का। जैसे मैं यह पाता हूं कि रिजर्व नेचर (इण्ट्रोवर्ट होना) बहुत बार मेरी घबराहट/चिन्ता का संवर्धक होता है और मैं उचित समय पर उचित लोगों से संप्रेषण नहीं कर पाता। यह बदलने का सयास यत्न किया है, पर वह शायद काफी नहीं है। इसी प्रकार सभी लोग अपनी विफलता से सीखने का यत्न कर सकते हैं। और तब विफलता का भय खाने की बजाय उससे सकारात्मकता निर्मित हो सकती है।
(यह तो फुटकर सोच है। अन्यथा, विफलता का भय तो ऐसा विषय है जिसपर अनन्त लिख कर और कुछ न कर इत्मीनान से असफल हुआ जा सकता है!)
कुहरे के बारे में पिछले दिनों बहुत कुछ झेला-सोचा-लिखा और सुना गया है मेरे रेलवे के परिवेश में। एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि जब कुछ दिखाई न दे रहा हो, तब ट्रेन चालक को पुख्ता जानकारी दिलाना कि वह कहां चल रहा है – एक महत्वपूर्ण सुरक्षा औजार है। इसी को ले कर एक कल एक कम्पनी वाले की ओर से पावरप्वाइण्ट प्रेजेण्टेशन था एक उपकरण के विषय में जो ग्लोबल-पोजिशनिंग सेटेलाइट्स का प्रयोग कर रेलगाड़ी के चालक को आगे कौन सा स्टेशन, पुल, लेवल क्रासिंग गेट या सिगनल आने वाला है, उसकी पूर्व सूचना प्राप्त कराता है। यह सूचना कोहरे के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। 
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का प्रयोग कर अनेकानेक प्रकार के बहुउपयोगी उपकरण सामने आयेंगे। यह फॉगसेफ उनमें से एक है।
Wednesday, December 10, 2008
प्रिय भैया खरी खरी जी,
प्रिय भैया खरी खरी जी,
आशा है आप कुशल से होंगे। मैने अपनी पिछली पोस्ट पर आपकी टिप्पणी देखी थी:
पते की बात लिखी है आपने रीता दीदी पर क्या आपने घायलो के लिये कुछ किया क्या? या ज्ञान जीजाजी ने????? या कुछ करेंगे क्या??????आपका प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है। कई लोग निस्वार्थ हो कर कुछ करने को समाज सेवा का भी नाम देते हैं। काफी मुश्किल है यह कार्य और अकेले में तो यह बहुत कठिन हो जाता है। ज्ञान की रेलवे की नौकरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत अनुभव दिये और बहुत आत्म-संतुष्टि भी। रेलवे में “महिला समाज सेवा एवं कल्याण समिति” जैसी संस्था है। यह “चाय-समोसा” समिति नहीं है।
| मैं नहीं चाहता था कि रीता पाण्डेय इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करें। पर उन्होंने व्यक्त करने का मन बना लिया तो मेरे पास विकल्प नहीं है उसे न प्रस्तुत करने का। इस पोस्ट में कई बातें ऐसी हैं जो मुझे अवसाद ग्रस्त कर देती हैं। मैं उन्हे भूलना चाहता हूं। मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा मजबूत इन्सान है। इस तथ्य को कुबूल करने में मुझे कोई झिझक नहीं है। |
रेल दुर्घटनायें तो रेल चलने से जुड़ी ही रहती हैं। किसी रेल दुर्घटना होने पर जब रेल कर्मचारी और अधिकारी साइट रेस्टोरेशन के लिये जूझ रहे होते हैं, तब महिला समिति पीड़ितों के लिये रक्तदान, भोजन का इन्तजाम और अन्य प्रकार से मदद का काम संभालती है। इसके अलावा मुझे याद है कि हम लोगों ने पैसा और सामान इकठ्ठा कर उड़ीसा के चक्रवात, पूर्वी तट पर आई सुनामी या कच्छ/भुज के भूकम्प के लिये सहायता भेजने का काम किया था। अनेक दिन हम सवेरे से देर शाम तक इस काम पर लग जाते थे। मेरे बच्चे कुछ बड़े हो गये थे, लिहाजा समय निकालने में इतनी परेशानी नहीं होती थी। भुज के भूकम्प के समय तो आस पास के मण्डलों से रेल महिलायें मौके पर जा कर खुद काम कर रही थीं। स्काउट-गाइड के बच्चे और किशोर हमारे इस बारे में विशेष सहायक होते हैं।
एक रेल दुर्घटना ने तो मेरे परिवार का जो नुक्सान किया है, वह शब्दों में समेटना मेरे लिये कठिन है। उस घटना का जिक्र मैं चिकित्सकों के व्यवहार की वजह से कर रही हूं। भुसावल में मेरा बेटा मौत से जूझता पड़ा था। सही निर्णय के अभाव में २२ घण्टे निकल गये। वहां इलाज की मूल सुविधायें नहीं थीं। तुरत सीटी-स्कैन (जिसकी सुविधा न थी) कर आगे का इलाज तय होना था। न्यूरो सर्जन वहां उपलब्ध न थे। पर अस्पताल वाले न कुछ कर रहे थे, न कोई वैकल्पिक योजना सोच पा रहे थे। हम उसे अपने रिस्क पर भुसावल से ले कर जळगांव पंहुचे – एक न्यूरोसर्जन के पास। वे न्यूरोसर्जन देवतुल्य थे हमारे लिये। ठीक इसी तरह इन्दौर के चोइथराम अस्पताल में जो डाक्टर मिले, वे भी देवतुल्य थे। उन्होंने मेरे बेटे के सिर का ऑपरेशन किया। हम उसके बाद मुम्बई के एक न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेने गये – बंगलोर में निमहंस जाने के पहले। ये सज्जन अपने एक एक मिनट का पैसा लेते थे पर जबान से जहर उगल रहे थे। उन्होंने हमें झटक दिया और हमने उन्हें। आखिर वे मेरे भगवान तो न थे! मेरे भगवान से जो बात हुई थी, उसके अनुसार उन्होंने हमें दिलासा दी थी कि हमारे जद्दोजहद की सीमा हमारी हार जीत का फैसला करेगी। और मैं अपनी जीत मान कर चल रही थी।
--- बात बम धमाके की हुई थी। बनारस में स्टेशन की लॉबी में और संकटमोचन के परिसर में बम फटे थे। ज्ञान उस दिन घर पंहुचे ही थे कि टीवी पर यह समाचार आने लगा। ये तो उल्टे पैर भागे। सड़क सेफ न लगी तो रेल पटरी के किनारे-किनारे पैदल चलते स्टेशन पंहुचे। ट्रेन के सघन तलाशी, घायलों को अस्पताल भेजना, मृत शरीर और अंगों को मोर्चरी रवाना करना; यह सब काम निपटा कर जब ज्ञान घर वापस आये तो रात के दो-तीन बज चुके थे।
एक दिन बाद हम अस्पताल गये घायलों को देखने। बहुत दर्दनाक दृश्य था। अचानक एक परिचित चेहरा दिखा। वह हमारे वाणिज्य विभाग का कर्मचारी था। उसके दोनो बेटे संकटमोचन के धमाके में घायल हो गये थे। बड़े को तो डिस्चार्ज कर दिया गया था फर्स्ट एड के बाद। पर छोटे का पैर बुरी तरह घायल था। डाक्टर साहब ने हमें बताया कि अगर उसका पैर काट दिया जाये तो शायद जान बच जाये। पिता भाव शून्य आंखों से देख रहा था। मैं चाह कर भी उस पिता को यह सलाह न दे पाई कि वह पैर का ऑपरेशन कराने दे। चार दिन बाद उस बेटे की मृत्यु हो गई। बारूद का जहर पूरे शरीर में फैल गया था।
तो भैया खरी खरी, यह मेरा अपना भोगा यथार्थ है। जिन्दगी की जद्दोजहद से खुरदरी जमीन पर चलने की आदत पड़ गई है। खरी खरी सुनने पर कभी कभी मौन टूट जाता है।
कभी इलाहाबाद आयें तो मिलियेगा।
आपकी बहन,
रीता पाण्डेय।
Friday, December 5, 2008
उधर भी झांक आते लोग
 मुम्बई हादसों ने सबके मन में उथल पुथल मचा रखी है। सब की भावनायें किसी न किसी प्रकार से अभिव्यक्त हो रही हैं। ज्ञान भी कुछ लिखते रहे (उनकी भाषा में कहें तो ठेलते रहे)। कुछ तीखा भी लिखते, पर उसे पब्लिश करने से अपने को रोकते रहे। उन्होंने मुझसे भी पूछा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? ईमानदारी से कहूं तो मेरे मन में निपट सन्नाटा था। अंतर्मन में कुछ घुमड़ रहा था, पर आकार नहीं ले पा रहा था।
मुम्बई हादसों ने सबके मन में उथल पुथल मचा रखी है। सब की भावनायें किसी न किसी प्रकार से अभिव्यक्त हो रही हैं। ज्ञान भी कुछ लिखते रहे (उनकी भाषा में कहें तो ठेलते रहे)। कुछ तीखा भी लिखते, पर उसे पब्लिश करने से अपने को रोकते रहे। उन्होंने मुझसे भी पूछा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? ईमानदारी से कहूं तो मेरे मन में निपट सन्नाटा था। अंतर्मन में कुछ घुमड़ रहा था, पर आकार नहीं ले पा रहा था। श्रीमती रीता पाण्डेयकी लिखी पोस्ट। आप उनके अन्य लेख "रीता" लेबल पर सर्च कर देख सकते हैं।
कई बार मुझे अपने सोचने के तरीके पर खुद को अजीब लगता है। जो मर गये, वे कैसे मरे, उन्हें किसने मारा, सुरक्षा नाकाम कैसे हुई – इस सब की चीर फाड़ होती है। पर दुर्घटना में जिनका एक पैर चला गया, हाथ चला गया, आंखें चली गयीं; उनके परिवार वाले उन्हें ले कर कैसे सामना कर रहे होंगे आगे की जिन्दगी का? मिलने वाले मुआवजे पर वकील और सरकारी अमला किस तरह
 गिद्ध की तरह टूट पड़ता होगा। कमीशन पर उनके केस लड़े जाते होंगे मुआवजा ट्रीब्यूनल में। और सहानुभूति की लहर खत्म होने पर डाक्टर लोग भी कन्नी काटने लगते हैं। इन सब बातों को भी उधेड़ा जाना चाहिये। मोमबत्ती जलाने वाले थोड़ा वहां भी झांक आते तो अच्छा होता।
गिद्ध की तरह टूट पड़ता होगा। कमीशन पर उनके केस लड़े जाते होंगे मुआवजा ट्रीब्यूनल में। और सहानुभूति की लहर खत्म होने पर डाक्टर लोग भी कन्नी काटने लगते हैं। इन सब बातों को भी उधेड़ा जाना चाहिये। मोमबत्ती जलाने वाले थोड़ा वहां भी झांक आते तो अच्छा होता। मुझे याद आ रही है वह लड़की जिसके ट्रेन विस्फोट में दोनो पैर उड़ गये थे। उस समय हम बनारस में थे। रेल सुरक्षा आयुक्त के साथ ज्ञान भी अस्पताल गये थे घायलों को देखने और उनसे हाल पूछने। उस लड़की के बारे में लोगों ने बताया था कि उसके मां-बाप पहले ही गुजर चुके हैं। वह अपनी बहन के घर जा रही थी कि यह हादसा हो गया ट्रेन में। ज्ञान ने सुरक्षा आयुक्त महोदय से कहा था - “सर, अगर आप इस जांच के दौरान अस्पताल का दो चार बार दौरा और कर लेंगे तो डाक्टर थोड़ा और ध्यान देंगे इस लड़की पर।”
घर आ कर ज्ञान ने मुझे इस लड़की के बारे में बताया। मुझे लगा कि यह लड़की बेचारी तो दो पाटों में फंस गई। मुआवजे में कमीशन तो वकील और सरकारी अमला ले जायेगा। बचा पैसा बहनोई रख लेगा, बतौर गार्जियन। एक गरीब लड़की, जिसके मां-बाप न हों, दोनो पैर न हों, वह इस बेदर्द दुनियां में कैसे जियेगी? मैने ईश्वर से प्रार्थना की – भले जीवन अमूल्य हो, पर भगवान उसे अपने पास बुला लो।
पता नहीं उस लड़की का क्या हुआ।
Wednesday, November 26, 2008
छोटे छोटे पिल्ले चार!
मेरे घर के सामने बड़ा सा प्लॉट खाली पड़ा है। अच्छी लोकेशन। उसके चारों ओर सड़क जाती है। किसी का है जो बेचने की जुगाड़ में है। यह प्लॉट सार्वजनिक सम्पत्ति होता तो बहुत अच्छा पार्क बन सकता था। पर निजी सम्पत्ति है और मालिक जब तक वह इसपर मकान नहीं बनाता, तब तक यह कचरा फैंकने, सूअरों और गायों के घूमने के काम आ रहा है।
रीता पाण्डेय की पोस्ट। आप उनकी पहले की पोस्टें रीता लेबल पर क्लिक कर देख सकते हैं। |
 सन्दीप के बताने पर भरतलाल ने अनुमान लगाया कि वह शायद बच्चा देने वाली है। दोनो ने वहां कुछ चिथड़े बिछा दिये। रात में कुतिया ने वहां चार पिल्लों को जन्म दिया। संदीप की उत्तेजना देखने लायक थी। हांफते हुये वह बता रहा था - कुलि करिया-करिया हयेन, हमरे कि नाहीं (सब काले काले हैं, मेरी तरह)| कुतिया बच्चा देने की प्रक्रिया में थी तभी मैने उसके लिये कुछ दाल भिजवा दी थी। सुबह उसके लिये दूध-ब्रेड और दो परांठे भेजे गये।
सन्दीप के बताने पर भरतलाल ने अनुमान लगाया कि वह शायद बच्चा देने वाली है। दोनो ने वहां कुछ चिथड़े बिछा दिये। रात में कुतिया ने वहां चार पिल्लों को जन्म दिया। संदीप की उत्तेजना देखने लायक थी। हांफते हुये वह बता रहा था - कुलि करिया-करिया हयेन, हमरे कि नाहीं (सब काले काले हैं, मेरी तरह)| कुतिया बच्चा देने की प्रक्रिया में थी तभी मैने उसके लिये कुछ दाल भिजवा दी थी। सुबह उसके लिये दूध-ब्रेड और दो परांठे भेजे गये।  रात में मेरी चिन्तन धारा अलग बह रही थी। सड़क की उस कुतिया ने अपनी डिलीवरी का इन्तजाम स्वयम किया था। कोई हाय तौबा नहीं। किसी औरत के साथ यह होता तो हड़कम्प मचता – गाड़ी/एम्ब्यूलेंस बुलाओ, डाक्टर/नर्सिंग होम का इन्तजाम करो, तरह तरह के इंजेक्शन-ड्रिप्स और जरा सी देर होती तो डाक्टर सीजेरियन कर चालीस हजार का बिल थमाता। फिर तरह तरह के भोजन-कपड़े-दवाओं के इन्तजाम। और पता नहीं क्या, क्या।
रात में मेरी चिन्तन धारा अलग बह रही थी। सड़क की उस कुतिया ने अपनी डिलीवरी का इन्तजाम स्वयम किया था। कोई हाय तौबा नहीं। किसी औरत के साथ यह होता तो हड़कम्प मचता – गाड़ी/एम्ब्यूलेंस बुलाओ, डाक्टर/नर्सिंग होम का इन्तजाम करो, तरह तरह के इंजेक्शन-ड्रिप्स और जरा सी देर होती तो डाक्टर सीजेरियन कर चालीस हजार का बिल थमाता। फिर तरह तरह के भोजन-कपड़े-दवाओं के इन्तजाम। और पता नहीं क्या, क्या।
प्रकृति अपने पर निर्भर रहने वालों की रक्षा भी करती है और उनसे ही इन्तजाम भी कराती है। ईश्वर करे; इस कुतिया के चारों बच्चे सुरक्षित रहें।
पुन: – कुतिया और बच्चों के लिये संदीप और भरतलाल ने एक घर बना दिया है। नियम से भोजन देते हैं। कुतिया कोई भी समस्या होने पर अपनी कूं-कूं से इन्हें गुहार लगाने पंहुच जाती है। वह जान गयी है कि यही उसका सहारा हैं। पिल्लों ने अभी आंख नहीं खोली है।




